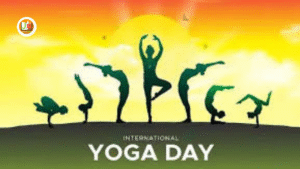भारतीय संविधान संहिताबद्ध एक दस्तावेज़ में लिखा गया है और एक ही निकाय द्वारा अधिनियमित किया गया है। भारतीय संविधान सर्वोच्च है, कठोरता और लचीलेपन का समामेलन है। हमारे समाज और राजनीति को बदलने वाले स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से संविधान बनाने के लिए बहुत सारी आम सहमति बनी। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? (Making of the Indian Constitution in Hindi) इसके बारे में ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु इस प्रकार हैं

- 1931 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान के विचार पर प्रस्ताव दिया गया था।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे बुनियादी मूल्यों को इस प्रस्ताव से वापस ले लिया गया था।
- औपनिवेशिक शासन के अनुभव ने भारत के लिए विधायी संस्थागत डिजाइन के विकास और विकास में मदद की।
भारतीय संविधान का निर्माण (Making of the Indian Constitution) यूपीएससी सीएसई का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस और UPSC मेन्स सिलेबस के बारे में अच्छे तरीके से जान लें और परीक्षा की तैयारी करें
भारतीय संविधान के निर्माण का कालक्रम | Timeline of Making of the Indian Constitution
| तिथियां | घटनाएं |
| 1934 | एमएन रॉय ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार दिया। |
| 1935 | संविधान सभा बनाने के इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया और एक मांग रखी गई। |
| 1938 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान सभा में केवल भारतीय शामिल हों। |
| 1940 | अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया |
| 1942 | भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) के बाद होगा। |
| 1946 | कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा के पास389 सीटें (296 ब्रिटिश भारत और 93 रियासतें)कांग्रेस द्वारा बहुमत सीटें-208 |
| 9 दिसंबर 1946 | 211 सदस्यों के साथ हुई संविधान सभा की पहली बैठकसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा थे। |
| 11 दिसंबर 1946 | स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद।उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जीसंवैधानिक सलाहकार बीएन राव |
| 13 दिसंबर 1946 | जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव जिसने संविधान की दार्शनिक संरचना को निर्धारित किया। इसे 22 जुलाई 1947 को पारित किया गया था |
| 3 जून 1947 | माउंटबेटन ने दो संविधान सभा की योजना बनाई।सीटों की संख्या घटकर 299 हो गई।प्रथम भारत की संसद – संविधान सभा का गठन किया गया था।स्वतंत्र भारत के प्रथम वक्ता- जी वी मालवणकरसंविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद। |
| 26 नवंबर 1949 | भारत का संविधान बना था |
भारतीय संविधान सभा की मांग | Demand for Constituent Assembly
- 1922 में एनी बेसेंट की आम सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने पर सहमति व्यक्त की।
- ब्रिटिश संसद को 1925 के भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक के साथ प्रस्तुत किया गया था। भारत के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों में से एक।
- मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसे पूर्ण संविधान की दिशा में पहला बड़ा प्रयास माना जाता था, 1928 में प्रकाशित हुई थी।
- 1930 और 1932 के बीच, संवैधानिक सुधार पर तीन गोलमेज बैठकें बुलाई गईं।
- 1934 में एमएन रॉय ने संविधान सभा का विचार रखा।
- 1935 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
- 1938 में, जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य होने चाहिए।
- 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। इसे अगस्त ऑफर का नाम दिया गया।
- 1942 में , सर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा। इसे क्रिप्स मिशन कहा गया।
- 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया।
संविधान सभा की संरचना | Composition of Constituent Assembly
- संविधान सभा में सीटों की कुल संख्या – 389 सीटें (292 सीटें – ब्रिटिश प्रांत और 93 सीटें – रियासतें)।
- ब्रिटिश प्रांतों को तीन प्रमुख समुदायों में विभाजित किया गया था जिसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य शामिल थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा विधानसभा के लिए चुना जाता था।
- बाद में, भारत के विभाजन के कारण कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई।
- चुनाव का तरीका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से था, जहां 1 सीट लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी।
संविधान सभा की विशेषताएं और कार्य | Features and Functions of the Constituent Assembly
- प्रांतों ने 292 सदस्यों का चुनाव किया, जिसमें भारतीय राज्यों को अधिकतम 93 सीटें प्राप्त हुईं।
- प्रत्येक प्रांत में सीटों को तीन मुख्य समितियों: मुस्लिम, सिख और जनरल के बीच उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में विभाजित किया गया था।
- प्रांतीय विधान सभा में, प्रत्येक समुदाय के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके अपने स्वयं के प्रतिनिधि चुनते हैं।
- रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा चुना जाना था।
- 13 दिसंबर, 1946 को, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के संविधान सभा के मिशन की शुरुआत की।
- संकल्प का लक्ष्य था “… भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करना और उसके भविष्य के प्रशासन के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना…”
- प्रस्ताव में बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित किया गया जो संविधान सभा के काम का मार्गदर्शन करेंगे। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया।
- रियासतों के प्रतिनिधि धीरे-धीरे इसमें शामिल हो गए। विधानसभा का गठन 28 अप्रैल, 1947 को छह राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ किया गया था।
- 3 जून, 1947 को देश के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद अन्य रियासतों के बहुमत के प्रतिनिधियों ने विधानसभा में अपनी सीट ग्रहण की।
संविधान का मसौदा तैयार करने और सामान्य कानूनों को अपनाने के अलावा निम्नलिखित कार्यों के लिए संविधान सभा जिम्मेदार थी :
इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता नामांकन में सुधार किया।
- 22 जुलाई 1947 को इसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी, 1950 को इसने राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को इसने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को चुना।
संविधान सभा की समितियां | Committees of Constituent Assembly
| प्रमुख समितियों का नाम | अध्यक्ष |
| संघ शक्ति समिति | पंडित जवाहरलाल नेहरू |
| संघ संविधान समिति | |
| राज्य समिति | |
| प्रांतीय समिति | सरदार वल्लभ भाई पटेल |
| मसौदा समिति | बी.आर. अम्बेडकर |
| सलाहकार समिति | सरदार वल्लभ भाई पटेल |
| नियम समिति | डॉ राजेंद्र प्रसाद |
| संचालन समिति |
मसौदा समिति | Drafting Committee
- इसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे।
- अक्टूबर 1948 में दूसरे मसौदे के बाद फरवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला मसौदा दिया गया था।
- अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को विधानसभा में पेश किया गया था।
- संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को मसौदा प्रस्ताव पारित किया गया था।
- दिसंबर 1939 में लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया।
- इस प्रकार, नागरिकता, चुनाव, अनंतिम संसद आदि से संबंधित कुछ प्रावधानों को छोड़कर, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ।
संविधान सभा की आलोचना | Criticism of Constituent Assembly
- प्रतिनिधि निकाय नहीं – क्योंकि यह सीधे निर्वाचित नहीं हुआ था।
- एक संप्रभु निकाय नहीं- जैसा कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था।
- इसे समय लेने वाला माना जाता था।
- माना जाता था कि इसमें कांग्रेस और हिंदुओं का वर्चस्व था।
स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन | Changes by Independence Act
- संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई और ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने का अधिकार था।
- इसने संविधान बनाने और एक विधायी निकाय के रूप में संसद के रूप में कार्य करने के दो कार्य किए।
- मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से हट गए और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया।
भारतीय संविधान के निर्माण का उद्देश्य संकल्प | Objective Resolution of Making of the Indian Constitution
- 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था जिसने संविधान की दार्शनिक संरचना को निर्धारित किया था।
- जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान को तैयार करने की आकांक्षाओं और मूल्यों को समझाया।
- इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
- यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है।
उद्देश्य संकल्प की विशेषताएं | Features of Objective Resolution
यह प्राप्त करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है –
- आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक सुरक्षा और राष्ट्र की तेज एकता।
- भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य राष्ट्र के रूप में घोषित करें।
- केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के साथ अपनी संघीय सरकार सुनिश्चित करें।
- भारत के नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विश्वास, आस्था पूजा और स्थान की गारंटी और सुरक्षा।
- पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, दलित वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना।
- भूमि, समुद्र और वायु पर क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता बनाए रखें।
- भारत को दुनिया में एक सही और सम्मानित स्थान प्राप्त करने में मदद करें जो विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देगा।